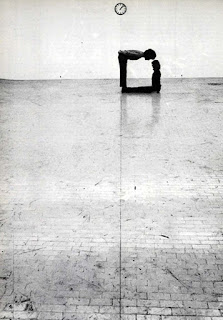विषय का चयन

लिखते हुए यह भी गौर करने लायक बात है, हम अक्सर किन विषयों पर लिखते हैं। यह चुनने से अधिक हमारे परिवेश पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता। एक हद तक यह एक महत्वपूर्ण कारक ज़रूर है। जब यह सवाल खुद से पूछता हूँ, तब लगता है, इस पर कभी बैठकर व्यवस्थित चिंतन नहीं किया। पहली नज़र में मुझे जो चीज़ लिखने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर करती है, वह बहुत सारे अतिरेकी क्षण हैं, जिनसे घिर जाने पर कह देना ही एक मात्र विकल्प बचता है। यह किसी भी तरह से कह देना है। जो भाव जैसा मेरे अंदर उतर रहा होता है, उसे उसके सबसे करीब जाकर कह देने में जो चुनौती है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दूसरे शब्दों में कहूँ, तब यह कुछ-कुछ वैसा ही है, जिसमें हम इस पल जिन भावों, अनुभूतियों से गुज़र रहे हैं, पढ़ने वाले को भी उन्हीं के पास लेकर आ पाने में जो संतुष्टि है, वह मुझे ऐसा बनाती रही है। जो मुझे पढ़ते हैं, लगातार लंबे समय से पढ़ते रहे हैं, वह भी ऐसा महसूस करते होंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, तब आप किसी भी पिछले पन्ने पर जाकर इस दलील की जाँच कर सकते हैं। लोग इस आत्मपरकता को दोष की तरह देखते हैं। जिस तरह के समय में हम